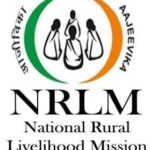समय के साथ पहाड़ में दीपावली का स्वरूप बदला

अनिल बहुगुणा अनिल (हिम तुंग वाणी)
समाज में लगातार आ रहे बदलाव ने रस्मोरिवाजों के साथ-साथ ही त्यौहारों को मनाने के ढ़ग में भी बदलाव ला दिए है। कभी उत्तराखण्ड में दीवाली का मतलब भैला व बग्वाल था। दशहरे के बाद पड़ने वाला हर त्यौहार दीवाली से जुड़ जाया करता था। लेकिन अब उत्तरखण्ड में भी दीवाली दीपावली हो गई है।
पूर्व में उत्तराखण्ड में मनाई जाने वाली बग्वाल के इतिहास में गाय के उपवास का जिक्र भी किया जाता है। और ठीक बग्वाल के दिन ही गाय के उपवास तोडने के लिए गाय के लिए अलग से मोटे अनाजो को उबाल कर उसके लिए पींडा तैयार किया जाता है।
सामाजिक मूल्यों को सहेज कर रखने वाला पहाड़ भी अब महज चयनीज दियों मे फंस गया है। कभी टिहरी उत्तरकाशी चमोली पौड़ी में अमावस्य में पड़ने वाली दीपावली के ठीक एक दिन पहले बग्वाल के नाम से दीवाली मनाई जाती थी जिसमें ग्रामीण अपने घरों में जिससे स्थानीय बोली में पूरी व उडद की दाल की पकोड़ी बना कर उन घरों में भेजी जाती थी जो अपने किसी प्रियजन की मौत के कारण त्यौहार मनाने से परहेज किया करते थे। रात को तिल के सूखे पेड़ों को जला कर पारंम्परिक वाद्यय यंत्रों के साथ एक खेल खेला जाता था जिसे भैले कहा जाता था। जिससे उस पूरे क्षे़त्र में तिल के सूखे पेड़ों के जलने के कारण देर रात तक उजाला रहा करता था।
टिहरी जिले में इस बग्वाल को रिख बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि टिहरी रियासत का एक सेना पति हूणों से लड़ते हुए तिब्बत में फंस गया था तब राजा ने उसे के आने तक दीवाली न मनाने का हुक्म जारी किया था एक माह बाद जब सेना पति अपनी सेना के साथ लौटा तब यहां बग्वाल मनाई गई तभी से इसे रिख बग्वाल के नाम से जाना जाता है।
दीवाली की यह पहाड़ी परम्परा अब उन्हीं गांवो तक सीमित रह गई है जो अभी भी खेती पर निर्भर है या खेती उन क्षेत्रों में हो रही है। क्योंकि भैले खेलने के लिए तिल के सूखे पेड़ों जैसे रौ मटीरियल की आवष्यकता होती है। इस त्यौहार में उसके अलावा और कुछ नहीं जलाया जाता है।